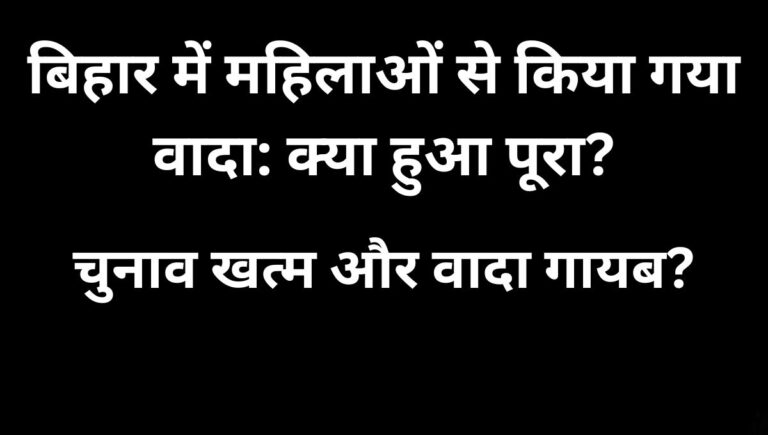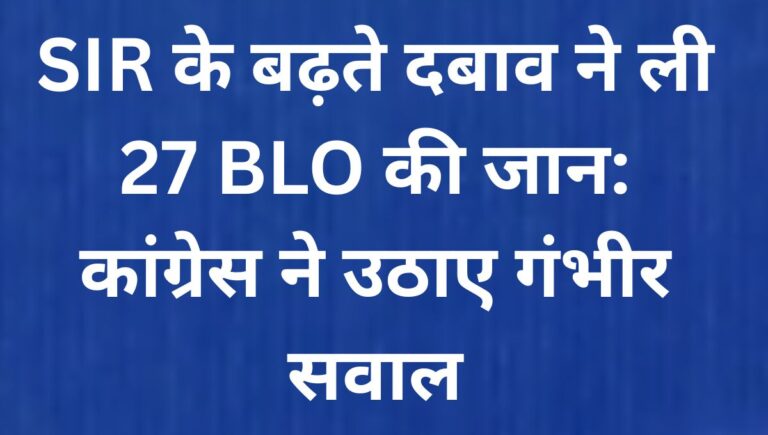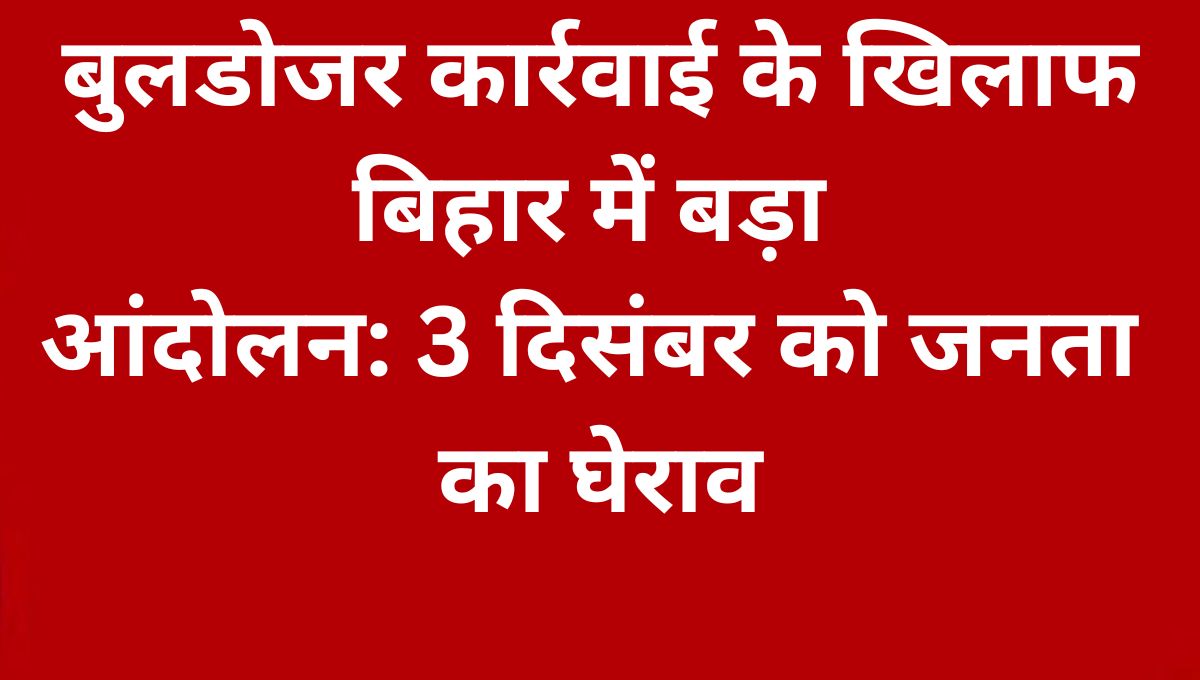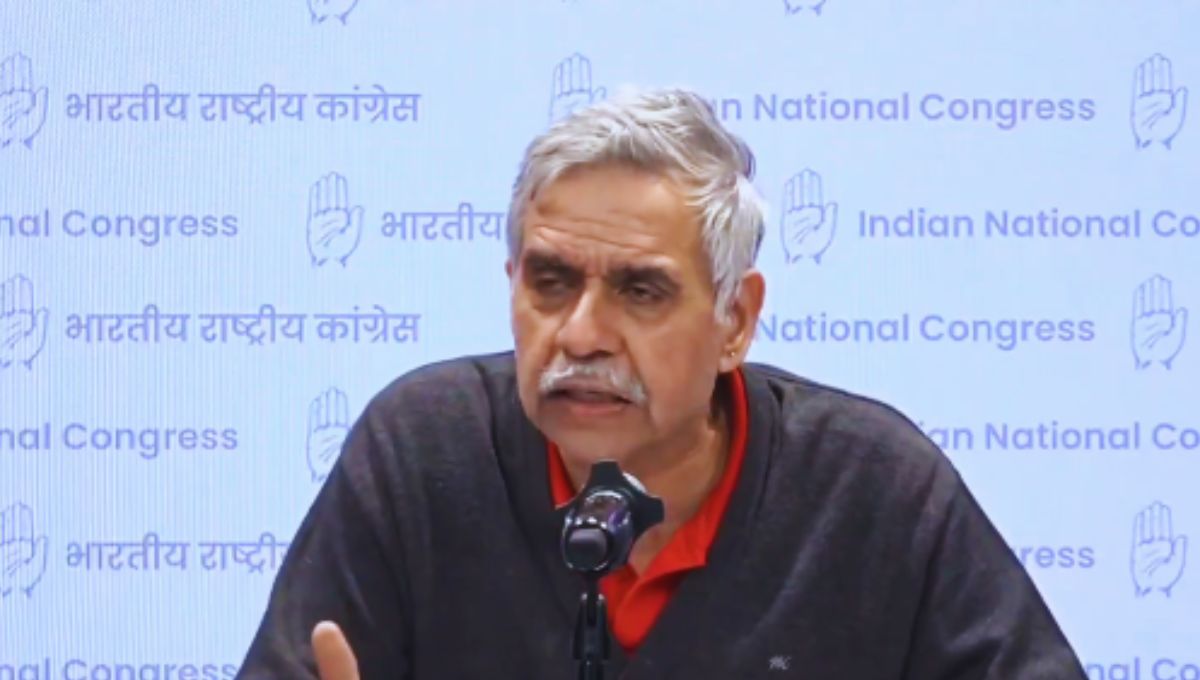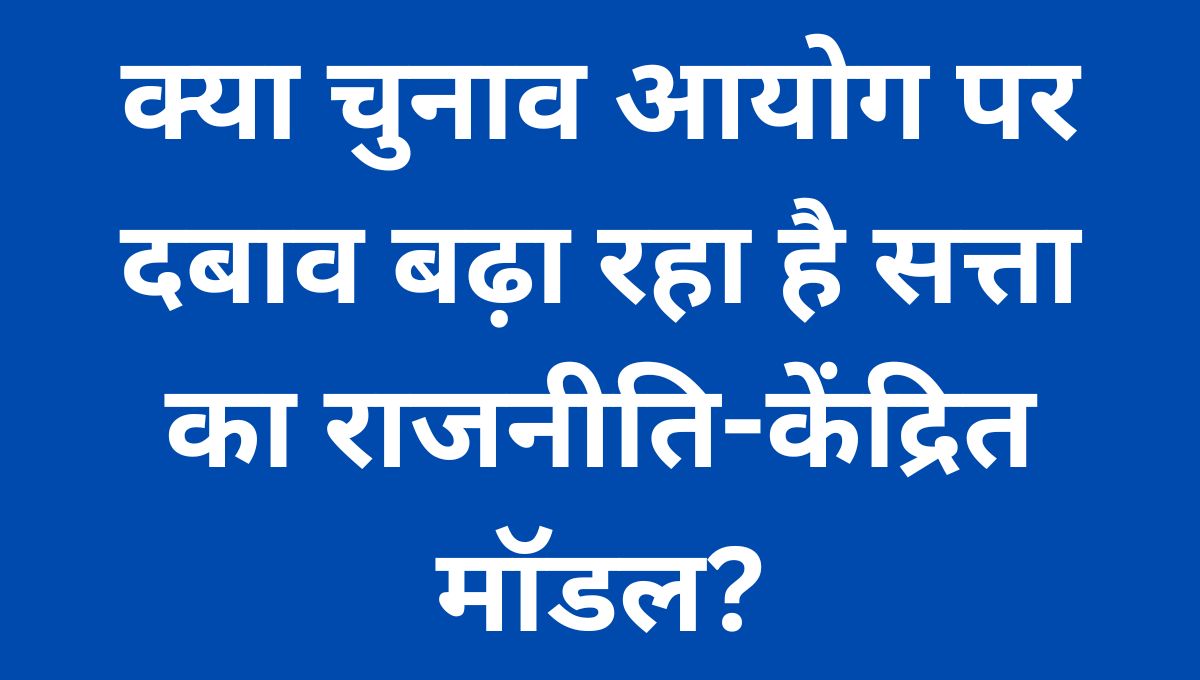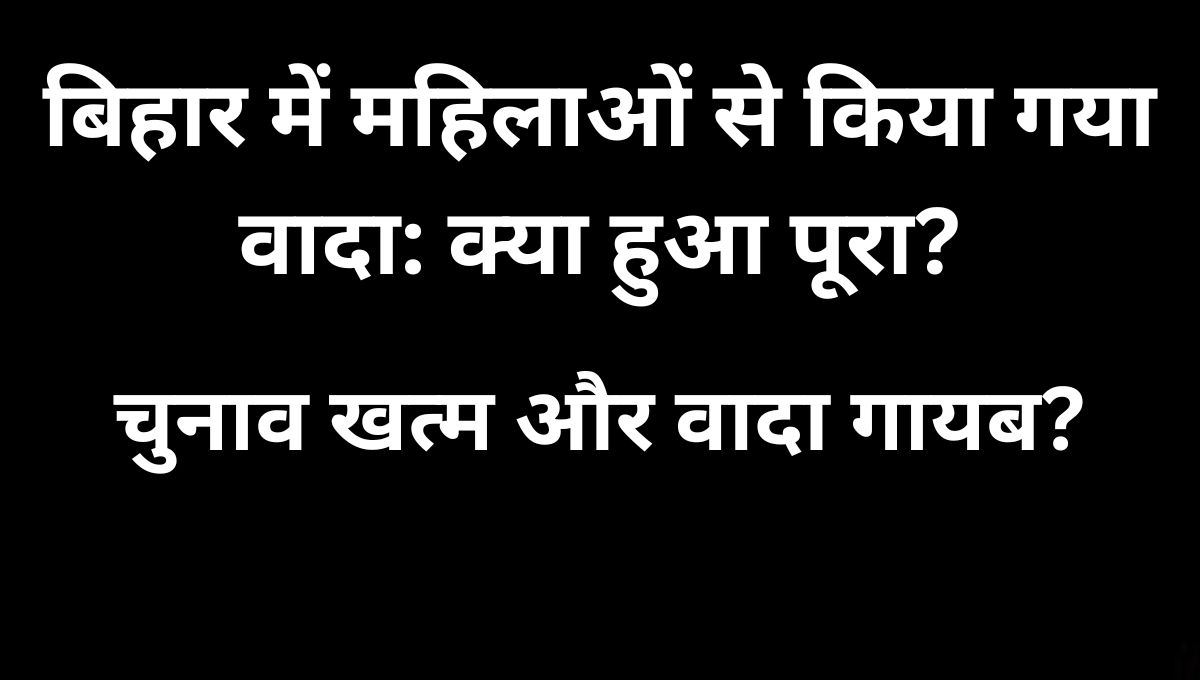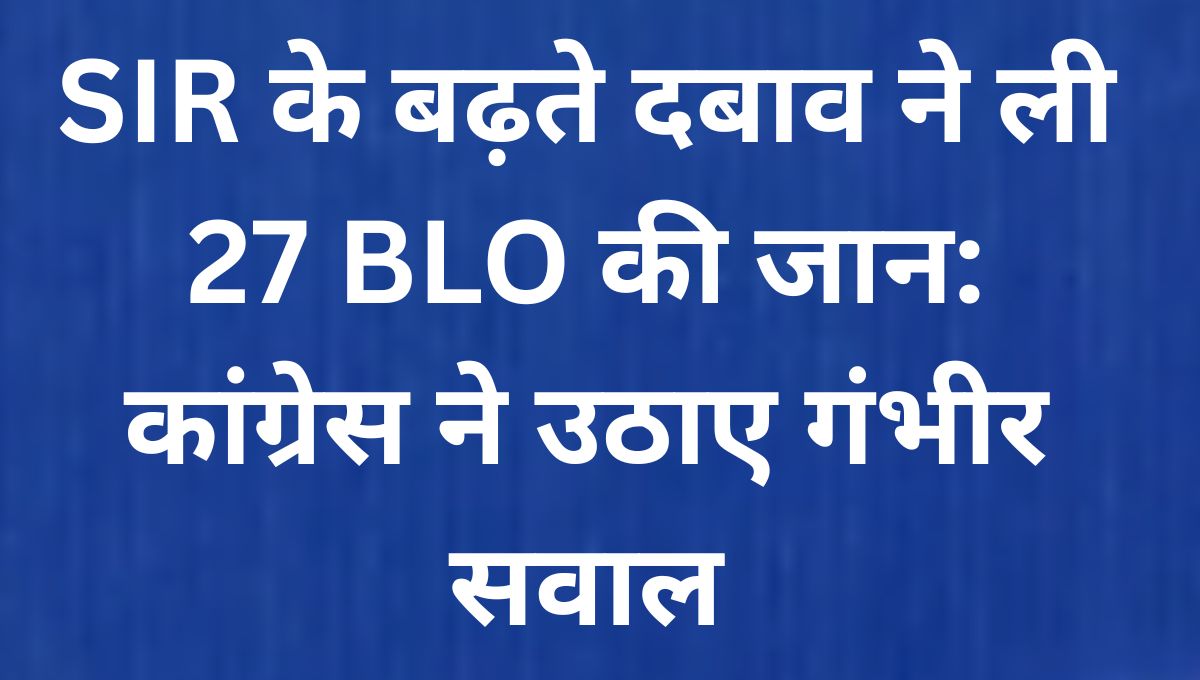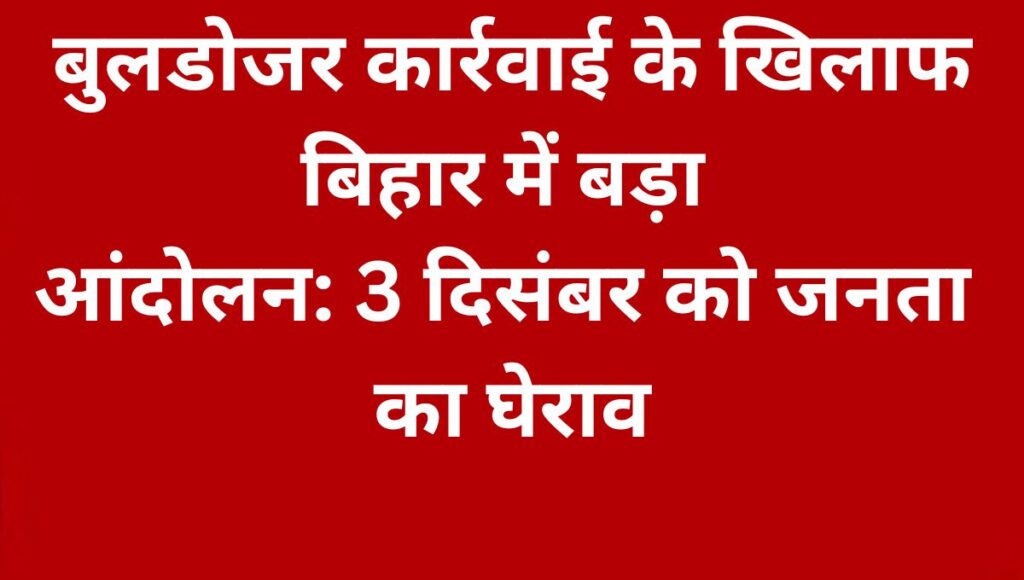बहुजन की चुप्पी और लोकतंत्र का मौन: क्या संविधान सभी के लिए है?
तीसरा पक्ष डेस्क,पटना :लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत नहीं होता बल्कि वह व्यवस्था है जो अल्पसंख्यकों वंचितों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है.भारत में संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार और गरिमा प्रदान किया है. परंतु जब हम बहुजन समाज की वास्तविक स्थिति पर नज़र डालते हैं तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है.बहुजन अर्थात अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक-सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़े समुदाय आज भी सामाजिक असमानता, उत्पीड़न और अवसरों की भारी कमी से जूझ रहे हैं.

जब इन वर्गों के अधिकारों का हनन होता है. जब उनकी जमीन छीना जाता है. जब उनके खिलाफ अत्याचार होता हैं. और तब भी देश का लोकतंत्र खामोश रहता है.तो यह सवाल उठता है: क्या लोकतंत्र अब बहुजन विरोधी हो चला है?
ये भी पढ़ें:
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बहुजनों का पद खाली क्यों? प्रशासनिक लापरवाही या सुनियोजित भेदभाव?
- मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला: भारत को चाहिए आर्थिक सुधारों की दूसरी क्रांति
बहुजन की चुप्पी: डर, अनुभव और विवशता
बहुजन समाज की चुप्पी कोई स्वैच्छिक निर्णय नहीं है. यह एक ऐतिहासिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार, और दमन की प्रक्रिया का परिणाम है. सदियों तक जातिगत भेदभाव ने इस समाज को हाशिए पर रखा गया जो बोले, उसे कुचल दिया गया। जो आगे बढ़ा, उसे नीचा दिखाया गया.
आज भी:
- दलितों पर अत्याचार की खबरें नियमित रूप से आती हैं. लेकिन उन पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई नहीं होता.
- आदिवासियों की ज़मीनें विकास के नाम पर छीन ली जाती हैं, और उन्हें माओवादी करार देकर गोलियों से सन्नाटा फैला दिया जाता है.
- OBC वर्ग को आर्थिक और शैक्षणिक संस्थानों में बराबरी नहीं मिलता है.
- इस सबके बीच अगर बहुजन समाज चुप है तो इसका कारण सिर्फ डर नहीं बल्कि न्याय तंत्र में विश्वास की कमी और सत्ता द्वारा उपेक्षा का लंबा इतिहास है.
लोकतंत्र की चुप्पी: सबसे बड़ा सवाल
लोकतंत्र, जिसे हम “जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार मानते हैं वह बहुजन के सवालों पर मौन क्यों है?
इस मौन के पीछे कई परतें हैं:
- सत्ताधारी वर्ग की भूमिका:
आज सत्ता पर काबिज़ वर्गों की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखें तो वे अक्सर ऊँची जातियों और संपन्न समुदायों से आते हैं. वे नीतियाँ बनाते हैं, कानून लागू करते हैं, परंतु उनकी प्राथमिकताओं में बहुजन हित शायद ही कभी सर्वोपरि होता हैं. - मीडिया का चयनात्मक दृष्टिकोण:
भारत का मुख्यधारा मीडिया बहुजन मुद्दों को तब तक नहीं दिखाता जब तक मामला सनसनीखेज या हिंसक न बन जाए. न शिक्षा, न रोज़गार, न आरक्षण से जुड़े प्रश्न,ये सब मीडिया की TRP में फिट नहीं बैठता है. - न्यायिक व्यवस्था का पक्षपात:
बहुजन उत्पीड़न के मामलों में अक्सर न्याय में देरी, दोषियों को सज़ा न मिलना, और पीड़ितों को संरक्षण न मिलना यह आम बात है. यह लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सीधा सवाल है. - विरोध को अराजकता कहना:
जब बहुजन समाज अपनी बात कहता है.धरना, प्रदर्शन, रैली या सोशल मीडिया के माध्यम से तो उसे “देशद्रोह”, “उपद्रवी” या “राजनीति से प्रेरित” कहकर खारिज कर दिया जाता
सामाजिक विषमता के संकेत
- संस्थानों में प्रतिनिधित्व की कमी: सरकारी नौकरियों, विश्वविद्यालयों, न्यायपालिका और मीडिया संस्थानों में बहुजन वर्गों की भागीदारी बहुत न्यूनतम न के बराबर है.
- भूमिहीनता और विस्थापन: आदिवासी और दलित समुदाय सबसे ज़्यादा विस्थापित होते हैं. खासकर विकास परियोजनाओं और खनन कार्यों के चलते.
- शिक्षा में असमानता: अच्छी शिक्षा अब भी एक वर्ग विशेष की पहुंच में है. जबकि सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था से सबसे ज़्यादा बहुजन बच्चे प्रभावित होते हैं.
समाधान क्या हैं?
- नीति और क्रियान्वयन में संवेदनशीलता:
सरकारी योजनाएँ जब तक बहुजन की ज़मीनी जरूरतों के अनुरूप नहीं बनेंगा और उन पर ईमानदारी से अमल नहीं होगा तब तक बदलाव संभव नहीं है. - शिक्षा और प्रतिनिधित्व:
शिक्षा ही असली मुक्ति का रास्ता है. बहुजन युवाओं को उच्च शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और नेतृत्व विकास के अवसर मिलने चाहिए. - सामाजिक आंदोलन की पुनर्रचना:
संगठित सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से बहुजन समुदाय को अपनी बात रखने की रणनीति अपनाना होगा.बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर, कांशीराम जैसे नेताओं की विचारधारा को फिर से लोकप्रिय बनाना होगा. - स्वतंत्र मीडिया और वैकल्पिक मंच:
बहुजन मुद्दों को उजागर करने के लिए वैकल्पिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, पॉडकास्ट, ब्लॉग और सोशल मीडिया चैनल एक सशक्त साधन बन सकता हैं.
निष्कर्ष: लोकतंत्र का असली चेहरा अब उजागर होना चाहिए
जब बहुजन समाज की आवाज़ को दबाया जाता है और लोकतंत्र की संस्थाएँ इस पर चुप रहता हैं.तो यह चुप्पी केवल तटस्थता नहीं, बल्कि एक साझेदार अपराध भी बन जाता है.
आज यह ज़रूरी है कि हम यह सवाल पूछें:
- बहुजन अगर चुप हैं तो डर से,पर लोकतंत्र अगर चुप है, तो किसके दबाव में?
- क्या यह चुप्पी सत्ता का डर है? या वह वर्गीय, जातीय गठजोड़ जो लोकतंत्र की आत्मा को खोखला कर रहा है?
- लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करने का समय आ चुका है. ताकि लोकतंत्र सिर्फ चुनावी शो नहीं, बल्कि न्याय और समानता का वास्तविक साधन बन सके.
I am a blogger and social media influencer. I am engaging to write unbiased real content across topics like politics, technology, and culture. My main motto is to provide thought-provoking news, current affairs, science, technology, and political events from around the world.